Biography of Vikram Sarabhai- डॉ॰ विक्रम अंबालाल साराभाई (12 अगस्त 1919 – 30 दिसंबर 1971) भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे। उन्होंने 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे और 40 संस्थान स्थापित किए। सन 1966 में, भारत सरकार ने इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्मभूषण से सम्मानित किया था।
डॉ॰ विक्रम साराभाई का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, और यह जगप्रसिद्ध है कि उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। हालांकि, उन्होंने अन्य क्षेत्रों जैसे वस्त्र, भेषज, आणविक ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक्स, और अन्य कई क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
वैज्ञानिक कौशल के इतिहास में, प्रसिद्ध गुजराती टाइकून अंबालाल साराभाई के वंशज विक्रम अंबालाल साराभाई ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। एक विद्वान भारतीय भौतिक विज्ञानी और खगोलीय विद्वान के रूप में पहचाने जाने वाले, डॉ. विक्रम अंबालाल साराभाई ने देश के वैमानिकी अन्वेषण निकाय की स्थापना करने और भारत में परमाणु ऊर्जा सुविधाओं के आगमन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भारत के ब्रह्मांडीय ओडिसी के चमकदार वास्तुकार के रूप में सम्मानित, उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह के प्रतिष्ठित सम्मान से अभिषिक्त किया गया था। उनके विलक्षण कारनामों की स्वीकृति में, विक्रम साराभाई को 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया, जो भारतीय नागरिक सम्मानों के समूह में प्रतिष्ठित थे।

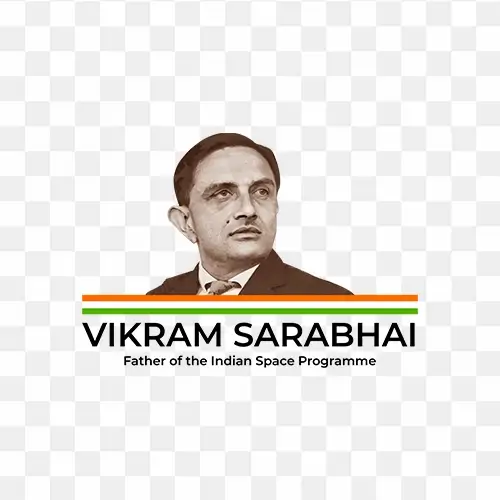

विक्रम साराभाई का शुरुआती जीवन- Vikram Sarabhai’s Early Life
डॉ॰ विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में एक समृद्ध जैन परिवार में हुआ था। उनके बचपन का समय “द रिट्रीट” नामक पैत्रिक घर में बिता, जहां अहमदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आकर गुजरते थे, और इसने साराभाई के व्यक्तित्व के विकास पर गहरा प्रभाव डाला। उनके पिता का नाम श्री अम्बालाल साराभाई और माता का नाम श्रीमती सरला साराभाई था।
विक्रम साराभाई की प्रारंभिक शिक्षा माता सरला साराभाई द्वारा शुरू की गई थी, जो मैडम मारिया मोन्टेसरी के पारिवारिक स्कूल में हुई। उन्होंने गुजरात कॉलेज से इंटरमीडिएट तक विज्ञान की शिक्षा पूरी की, और फिर 1937 में कैम्ब्रिज, इंग्लैंड की ओर रुख किया, जहां उन्होंने 1940 में प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोज डिग्री हासिल की।
द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान, विक्रम साराभाई ने भारत लौटकर बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में नौकरी शुरू की, जहां उन्होंने महान वैज्ञानिक चन्द्रशेखर वेंकटरमन के निरीक्षण में ब्रह्मांड किरणों पर अनुसंधान किया। उन्होंने अपना पहला अनुसंधान लेख “टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कास्मिक रेज़” भारतीय विज्ञान अकादमी की कार्यविवरणिका में प्रकाशित किया।
1940-45 की अवधि के दौरान, साराभाई ने कॉस्मिक रे पर अनुसंधान किया, जिसमें उन्होंने बंगलौर और कश्मीर-हिमालय में उच्च स्तरीय केंद्रों के गेइजर-मूलर गणकों के साथ कॉस्मिक रे के समय-रूपांतरणों का अध्ययन किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त होने पर, उन्होंने कैम्ब्रिज लौटकर अपनी डाक्ट्रेट पूरी की और 1947 में उष्णकटीबंधीय अक्षांक्ष (ट्रॉपीकल लैटीच्यूड्स) में कॉस्मिक रे पर अपने शोधग्रंथ के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्हें डाक्ट्रेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
इसके बाद, विक्रम साराभाई ने भारत में विज्ञान के क्षेत्र में अपना अनुसंधान जारी रखा, जिसमें उन्होंने अंतर-भूमंडलीय अंतरिक्ष, सौर-भूमध्यरेखीय संबंध, और भू-चुम्बकत्व पर अध्ययन किया।
विक्रम साराभाई की उपलब्धियाँ- Vikram Sarabhai Achievements
डॉ. विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में एक दूरदर्शी संस्थान निर्माता की भूमिका में अपने प्रतिष्ठान्वित पैरों के निशान छोड़े। 1947 में कैम्ब्रिज से लौटने के बाद, उन्होंने अपने अहमदाबाद निवास के पास एक शोध संस्थान स्थापित करने के लिए दोस्तों और परिवार से सहारा मांगा। इस प्रकार, केवल 28 वर्ष की आयु में, उन्होंने 11 नवंबर, 1947 को अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) की नींव रखी। पीआरएल, साराभाई द्वारा बनाए गए कई संस्थानों में से पहला, 1966 से 1971 तक उनके नेतृत्व में था।
वैज्ञानिक खोज के क्षेत्र के पार, विक्रम साराभाई ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद अपने परिवार के औद्योगिक उद्यम में सक्रिय भूमिका निभाई। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना करते हुए, उन्होंने 1956 तक महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश में कुशल प्रबंधन पेशेवरों की तत्परता को देखते हुए, साराभाई ने 1962 में अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (इंकोस्पर), जिसे बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) में बदला गया, विक्रम साराभाई के प्रयासों का अंगीकार है, जो 1962 में हुआ। 1966 में प्रिय भौतिक वैज्ञानिक होमी भाभा के निधन के बाद, साराभाई को भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। उनके प्रयासों में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना शामिल है। विशेष रूप से, साराभाई ने स्वतंत्रता के लिए स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी मंच को उनका गहरा प्रभाव दिखता है।
विक्रम साराभाई द्वारा खोजे गए अन्वेषण- Explorations Unearthed by Vikram Sarabhai
विक्रम साराभाई, देश भर में असंख्य संस्थानों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, डॉ. विक्रम साराभाई द्वारा संचालित उल्लेखनीय नींवों की कहानी को स्पष्ट करते हैं।
1947 के प्रारंभिक वर्ष में, उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) की आधारशिला रखी, जो अंतरिक्ष और सहवर्ती विज्ञान के लिए समर्पित एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित हुई।
11 दिसंबर, 1961 को अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की स्थापना ने देश के भीतर प्रबंधन संस्थानों के क्षेत्र में सर्वोपरि शीर्ष के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया।
बिहार के जादुगुड़ा में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) का 1967 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वावधान में उदय हुआ।
विक्रम ए साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र (वीएएससीएससी), जिसका नाम 1960 में अहमदाबाद में रखा गया था, खुद को समझदार लोगों के बीच विज्ञान और गणित की शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित करता है, वैज्ञानिक शिक्षा में पद्धतियों को बढ़ाने और नवीन करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
विक्रम साराभाई और उनकी पत्नी द्वारा अहमदाबाद में 1949 में स्थापित दर्पण प्रदर्शन कला अकादमी, पिछले तीन दशकों से उनकी संतान मल्लिका साराभाई के नेतृत्व में संचालित की जा रही है।
कलपक्कम में फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (एफबीटीआर), इसकी प्रारंभिक नींव 1985 में रखी गई थी, जो तेज ईंधन रिएक्टरों और सामग्रियों के लिए एक क्रूसिबल के रूप में कार्य करता है।
1967 में हैदराबाद के उपजाऊ मैदान में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) इलेक्ट्रॉनिक्स में एक मजबूत स्वदेशी इमारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसका प्रारंभिक अस्तित्व 21 नवंबर, 1963 से है, इसरो के देवालय में एक महत्वपूर्ण गढ़ के रूप में बड़ा है, जो भारतीय उपग्रह कार्यक्रम के लिए वैमानिकी और स्थानिक नलिकाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
अहमदाबाद में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी), जिसका उद्घाटन अध्याय 1972 में लिखा गया था, इसरो के दृष्टिकोण और मिशन को प्रकट करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है।
कलकत्ता में वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट (वीईसीसी), जिसकी कल्पना 1972 में की गई थी, परमाणु कण त्वरक के शोधन के साथ-साथ बुनियादी और व्यावहारिक परमाणु विज्ञान की खोज में परिश्रमपूर्वक संलग्न है।
विक्रम साराभाई के आविष्कार/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
विक्रम साराभाई के बारे में उपलब्धि का सबसे उच्च स्तर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की स्थापना माना जाता है। लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट पूरा करके 1947 में भारत लौटने के बाद, साराभाई ने नए गठित स्वतंत्र भारत सरकार को भारत के जैसे विकसित देश के लिए एक अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्णता को समझाने में सफलता प्राप्त की। डॉ. साराभाई को डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने समर्थन किया, जो किसे भारतीय परमाणु विज्ञान कार्यक्रम के पिता के रूप में स्वीकृत किया जाता है। साथ ही, उन्होंने भारत में पहले रॉकेट लॉन्च स्टेशन की स्थापना करने में डॉ. साराभाई का समर्थन किया।
21 नवंबर, 1963 को, एक उदार प्रयास के बाद, थुम्बा के पास अरब सागर के तट पर पहला रॉकेट लॉन्च सेंटर स्थापित किया गया। इस महत्वपूर्ण पहली उड़ान में सोडियम वेपर पेलोड के साथ हुआ। इस साफल्य के पीछे ढांचे की स्थापना, कर्मियों को जोड़ना, संचार संबंध स्थापित करना, और लॉन्च पैड निर्मित करने में एक उच्च प्रयास था। डॉ. विक्रम साराभाई ने अन्य प्रमुख देशों के अंतरिक्ष संगठनों के साथ नासा जैसी नाकारात्मक बातचीत में निरंतर शामिल रहे, जिससे जुलाई 1975 से जुलाई 1976 तक सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट (SITE) का प्रक्षेपण हुआ।
डॉ. साराभाई ने विज्ञान शिक्षा में अद्वितीय प्रेरणा के लिए 1956 में अहमदाबाद में सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की, जिसे विक्रम साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र (VASCSC) के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही, उन्होंने एक भारतीय उपग्रह के विकास और प्रक्षेपण के लिए एक परियोजना शुरू की। हालांकि उन्होंने भारत के पहले उपग्रह, आर्यभट्ट को साकार करने के लिए उत्साह से काम किया, लेकिन उनकी दुखद मृत्यु से चार साल पहले ही उसका प्रक्षेपण हो गया।
उनके अमूल्य योगदान की पहचान में, डॉ. विक्रम साराभाई को 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, जो उनके जीवन और उनकी छोड़ी गई सांगीतिक विरासत की स्मृति के रूप में था।
डॉ॰ विक्रम साराभाई: भारतीय विज्ञान के प्रेरणास्त्रोत- Inspiration of Indian Science
जनवरी 1966 में डॉ॰ होमी जे. भाभा के निधन के बाद, डॉ॰ विक्रम साराभाई को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने का कार्य सौंपा गया। साराभाई ने सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अनेक गतिविधियों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी की व्यापक क्षमताओं को पहचाना। इन गतिविधियों में संचार, मौसम विज्ञान, मौसम संबंधी भविष्यवाणी और प्राकृतिक संसाधनों के लिए अन्वेषण शामिल थे।
अहमदाबाद में स्थापित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने उनके नेतृत्व में अंतरिक्ष विज्ञान और बाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान का मार्ग दिखाया। साराभाई ने भारतीय रॉकेट प्रौद्योगिकी को भी प्रोत्साहित किया और भारत में उपग्रह टेलीविजन प्रसारण के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाई।
उन्होंने भारतीय भेषज उद्योग को भी प्रेरित किया और इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों के साथ मिलकर गुणवत्ता के उच्च मानक स्थापित करने का समर्थन किया। साराभाई ने इलेक्ट्रानिक आंकड़ा प्रसंस्करण और संचालन अनुसंधान तकनीकों को भेषज उद्योग में लागू किया और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक दवाइयों और उपकरणों को देश में ही विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विज्ञान की शिक्षा को सुधारने के लिए सामुदायिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना की और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी गहरी रूचि रखी।
1971 में तिरुवनन्तपुरम (केरल) के कोवलम में उनके देहांत के बाद, उनके सम्मान में तिरुवनंतपुरम में स्थापित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लाँचिंग स्टेशन (टीईआरएलएस) का नामकरण हुआ और सम्बद्ध अंतरिक्ष संस्थाओं का नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र रखा गया। इससे यह इसरो के एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र के रूप में उभरा और 1974 में सिडनी स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ ने निर्णय लिया कि ‘सी ऑफ सेरेनिटी’ पर स्थित बेसल नामक मून क्रेटर अब साराभाई क्रेटर के नाम से जाना जाएगा।
1972 में उनकी मृत्यु की पहली बरसी पर भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया गया।